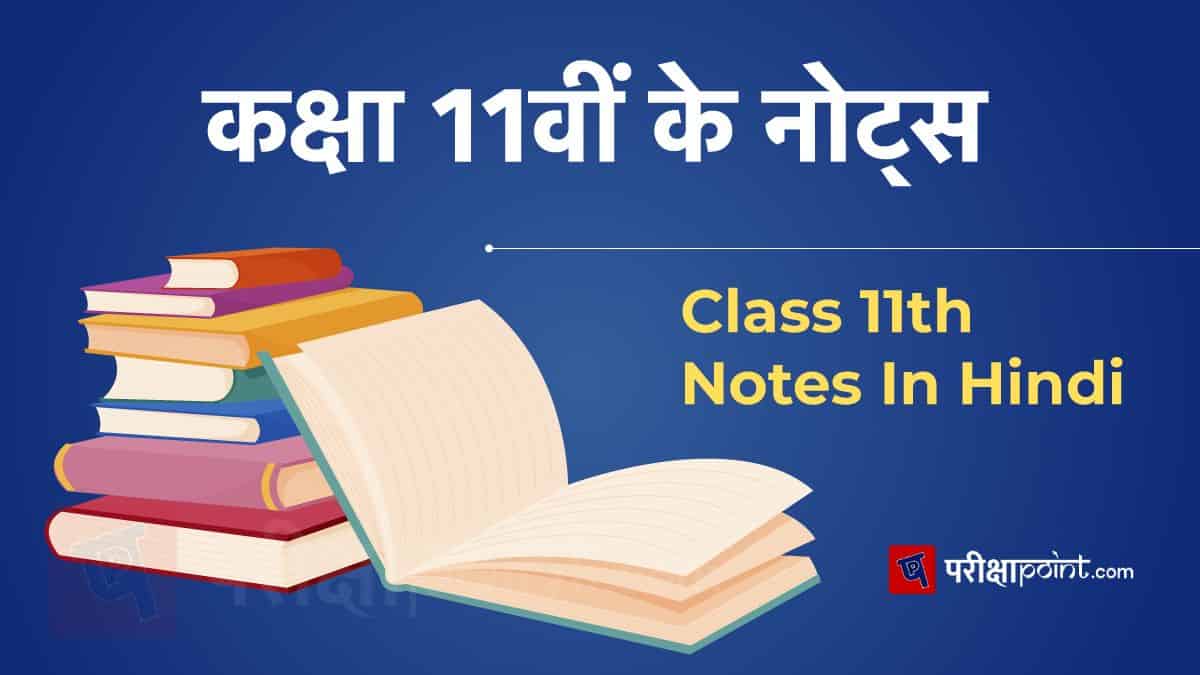इस लेख में छात्रों को एनसीईआरटी 11वीं कक्षा की भूगोल की पुस्तक-2 यानी “भारत भौतिक पर्यावरण” के अध्याय-4 “जलवायु” के नोट्स दिए गए हैं। विद्यार्थी इन नोट्स के आधार पर अपनी परीक्षा की तैयारी को सुदृढ़ रूप प्रदान कर सकेंगे। छात्रों के लिए नोट्स बनाना सरल काम नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों का काम थोड़ा सरल करने के लिए हमने इस अध्याय के क्रमानुसार नोट्स तैयार कर दिए हैं। छात्र अध्याय 4 भूगोल के नोट्स यहां से प्राप्त कर सकते हैं।
Class 11 Geography Book-2 Chapter-4 Notes In Hindi
आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दो ही तरह से ये नोट्स फ्री में पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने के लिए इस पेज पर बने रहें और ऑफलाइन पढ़ने के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें। एक लिंक पर क्लिक कर आसानी से नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए ये नोट्स बेहद लाभकारी हैं। छात्र अब कम समय में अधिक तैयारी कर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे, यह अध्याय पीडीएफ के तौर पर भी डाउनलोड हो जाएगा।
अध्याय- 4 “जलवायु”
| बोर्ड | सीबीएसई (CBSE) |
| पुस्तक स्रोत | एनसीईआरटी (NCERT) |
| कक्षा | ग्यारहवीं (11वीं) |
| विषय | भूगोल |
| पाठ्यपुस्तक | भारत भौतिक पर्यारवण |
| अध्याय नंबर | चार (4) |
| अध्याय का नाम | जलवायु |
| केटेगरी | नोट्स |
| भाषा | हिंदी |
| माध्यम व प्रारूप | ऑनलाइन (लेख) ऑफलाइन (पीडीएफ) |
कक्षा- 11वीं
विषय- भूगोल
पुस्तक- भारत भौतिक पर्यावरण
अध्याय-4 “जलवायु”
- ऐसी जलवायु जिसमें ऋतु के आधार पर पवनों की दिशा में अंतर होता है, मौसम कहलाता है। मौसम का परिवर्तन जल्दी होता है, जलवायु परिवर्तन में समय लगता है।
मानसून जलवायु की एकरूपता एवं विविधता
- दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाने वाली उष्ण मानसूनी जलवायु भारत में भी है।
- भारत में प्रादेशिक स्तर पर भी जलवायु में भिन्नता देखी जाती है, जैसे दक्षिण के केरल या तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तरप्रदेश और बिहार से अलग है।
- यह अंतर एक स्थान से दूसरे स्थान और क्षेत्रों में भी पाया जाता है।
- वर्षण के आधार पर भी भिन्नता देखी जाती है, हिमालय आदि क्षेत्रों में वर्षण बर्फ के रूप में और अन्य भागों में यह वर्षा के रूप में ही होती है।
जलवायु भिन्नता के कारक तत्व
- स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारक
- अक्षांश
- हिमालय पर्वत
- जल स्थल का वितरण
- समुद्र तट से दूरी
- समुद्र तल से ऊंचाई
- उच्चावच
- वायुदाब और पवनों से जुड़े कारक
- वायुदाब और पवनों का धरातल पर वितरण
- जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण
- पश्चिमी चक्रवर्तीय विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात
भारत में मानसून की प्रकृति
- यह एक जलवायवीय घटक है, इसका अध्ययन भूमंडलीय स्तर पर किया जाता है। मानसून की प्रकृति को इस तरह समझा जाता है-
- मानसून का आरंभ– 19वीं शताब्दी की व्याख्या के अनुसार गर्मी में समुद्र और स्थल गर्म होकर ताप के जरिए मानसूनी पवनों को उपमहाद्वीप की ओर भेजती हैं, जब सूरज अप्रैल और मई के महीने में कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, तब हिंदमहासागर के पास की भूमि गर्म हो जाती है, जिससे उपमहाद्वीप का उत्तर-पश्चिमी भाग न्यून दाब क्षेत्र बनाता है।
- भारत में मानसून का प्रवेश 1 जून को केरल के तट पर होता है, जो 10 जून तक आर्द्र पवनों को मुंबई तक पहुँचा देता है। जुलाई तक आते-आते पूरा उपमहाद्वीप मानसून के प्रभाव में आ जाता है।
- वर्षा लाने वाले तंत्र– पहला तंत्र उष्णकटिबंधीय अवदाब, दूसरा अरब सागर से उठने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसून धारा।
- मानसून का विच्छेद– जब दक्षिण-पश्चिम मानसून काल में कुछ समय वर्षा के बाद, आने वाले कुछ सप्ताह तक यदि बारिश न हो तो इसे ही मानसून विच्छेद कहा जाता है।
- मानसून का निर्वितरण– जब मानसून लौट जाता है या पीछे हट जाता है, इस परिस्थिति को मानसून का निर्वितरण कहा जाता है।
ऋतुएं
- भारत की ऋतुओं को चार भागों में बांटा गया है-
- शीत– भारत में इसकी शुरुआत नवंबर के महीने में होती है, जनवरी का महीना उत्तरी क्षेत्रों में सबसे ठंडा महीना होता है, उत्तर भारत के अधिकांश भागों में इस समय तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह तापमान कुछ क्षेत्रों में 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
- वायुदाब तथा पवनें- सूरज दिसंबर के अंत तक मकर रेखा पर दक्षिण गोलार्ध में सीधा चमकता है, वायु दाब दक्षिण भारत में अधिक नहीं होता।
- ग्रीष्म– मार्च में सूरज कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, अप्रैल और मई में उत्तर भारत में गर्मी चरम पर होती है। इस समय अधिकांश स्थानों पर तापमान 30 से 32 डिग्री हो जाता है। दक्षिण भारत में गर्मी उत्तर के मुकाबले कम होती है। ऐसा समुद्र के नजदीक स्थित होने के कारण होता है। दक्षिण का तापमान 26 से 32 डिग्री तक ही रहता है।
- वायुदाब तथा पवनें- उत्तरी भाग में अधिक गर्मी और कम वायु दाब पाया जाता है।
- दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु- मई के महीने में गर्मी के कारण निम्न वायु दाब बढ़ने लगता है, जो जून आते-आते बढ़ जाता है जिससे हिन्द महासागर की पवनें आकर्षित होती हैं। ये अपने साथ आर्द्रता लेकर आती हैं, जिससे अचानक बारिश होती है। इस समय में दिन के तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है।
भू-खंड पर मानसून दो शाखाओं में पहुंचता है-
- अरब सागर की मानसून पवनें– इसकी एक शाखा पश्चिमी घाट से आती है, दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदी की घाटियों से होकर मध्य भारत में प्रवेश करती है। तीसरी शाखा कच्छ और सौराष्ट्र प्रायद्वीप से टकराती है।
- बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें– ये पवनें म्यांमार और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व के थोड़े से हिस्से से टकराती हैं। अराकान पहाड़ियाँ इसके बड़े हिस्से को भारत के उपमहाद्वीप की ओर मोड़ देती हैं।
- मानसून वर्षा की विशेषताएं–
- मानसून की वर्षा मुख्यतः उच्चावच और भू-आकृति द्वारा नियंत्रित की जाती है।
- जैसे-जैसे मानसून की दूरी समुद्र से बढ़ती है, मानसून की वर्षा घटने लगती है।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा कोलकाता में अधिक और दिल्ली में कम होती जाती है।
- ग्रीष्मकालीन वर्षा का मृदा का अपरदन होता है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्ययवस्था में भी मानसून का महत्व है।
- मानसून के निवर्तन की ऋतु- मानसून का निवर्तन अक्टूबर-नवंबर में हो जाता है। सितंबर के पहले हफ्ते में मानसून राजस्थान के पश्चिमी हिस्से से लौटता है। इस समय में तापमान बढ़ने लगता है, लेकिन जमीन की आर्द्रता बनी रहती है। इस समय को ‘कार्तिक मास की ऊष्मा’ कहा जाता है।
- अक्टूबर के महीने में तापमान में तेज गिरावट होती है, जिससे उत्तर भारत में ठंड महसूस की जाती है, यहाँ मौसम सूखा हो जाता है और प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्सों में वर्षा होती है।
भारत की परंपरागत ऋतुएं
- उत्तरी और मध्य भारत में भिन्न ऋतु चक्र के आधार पर ऋतुओं का वितरण किया जाता है, यह ऋतु व्यवस्था दक्षिण भारत में अलग है-
| ऋतु | भारतीय परंपरा अनुसार महीने | अंग्रेजों द्वारा निर्मित कैलेंडर |
| बसंत ऋतु | चैत्र-बैसाख | मार्च-अप्रेल |
| ग्रीष्म | ज्येष्ठ-आषाढ़ | मई-जून |
| वर्षा ऋतु | श्रावण-भाद्र | जुलाई-अगस्त |
| शरद ऋतु | आश्विन-कार्तिक | सितंबर-अक्टूबर |
| हेमंत ऋतु | मार्गशीर्ष-पौष | नवंबर-दिसंबर |
| शिशिर ऋतु | माघ-फाल्गुन | जनवरी-फरवरी |
वर्षा वितरण
- मापन के आधार पर पता चलता है कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा 125 सेमी है।
- यह भिन्न हिस्सों में भिन्न मात्रा में दर्ज की जाती है-
- अधिक वर्षा क्षेत्र- इन इलाकों में 200 सेमी से भी ज्यादा बारिश दर्ज की जाती है, ये क्षेत्र हैं- मेघालय की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट।
- मध्यम वर्षा क्षेत्र– इसमें गुजरात का दक्षिण भाग, तमिलनाडु, ओडिशा के साथ-साथ, उत्तर-पूर्वी प्रायद्वीप आदि क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में 100 से 200 सेमी तक बारिश होती है।
- न्यून वर्षा क्षेत्र– यहाँ 50 से 100 सेमी तक ही वर्षा होती है। दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर-प्रदेश, दक्कन के पठार, गुजरात आदि क्षेत्र इसमें आते हैं।
- अप्रयाप्त वर्षा क्षेत्र– इन क्षेत्रों में 50 सेमी से भी कम बारिश दर्ज की जाती है, प्रायद्वीप के कुछ हिस्से महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि के कुछ हिस्से इसके अंतर्गत आते हैं।
भारत में जलवायु प्रदेश
- भारत में मानसून प्रकार की जलवायु होने के कारण, यहाँ की क्षेत्रीय भिन्नता का पता लगाया जा सकता है, जो जलवायु प्रदेश पहचानने में सहायक है।
- तापमान और वर्षा को जलवायु के वर्गीकरण में निर्णायक माना जाता है। भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकार हैं-
- उष्णकटिबंधीय जलवायु
- शुष्क जलवायु
- गर्म जलवायु
- हिम जलवायु
- बर्फीली जलवायु
भारत का मानसून आधारित आर्थिक जीवन
- भारत में आने वाले दक्षिण-पश्चिम मानसून से इसकी कृषि समृद्ध होती है, जिसपर भारत की 64% जनता निर्भर है।
- मानसून में पाई जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नता से कई प्रकार की फसलें उगाईं जाती हैं।
- वर्षा के न होने का कृषि पर बुरा प्रभाव होता है, यह ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक है जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं।
- जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता, कई मायनों जैसे- कपड़े, आवास और भोजन से पता लगाई जा सकती है।
भूमंडल का तापन
- वैश्विक स्तर पर भूमंडल के ताप में वृद्धि होती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इस समस्या को ओर भी बढ़ा रहा है।
- इस तरह की अन्य गैसें जो तापवृद्धि का कारण हैं, को ही ग्रीनहाउस गैसें कहा जाता है।
- पिछले 150 सालों में धरती का औसत तापमान बढ़ा है। वर्ष 2100 तक यह तापमान 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा, जिससे ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्र तल बढ़ेगा।
- इन सबके परिणामस्वरूप बाढ़ों की संख्या बढ़ेगी, जिससे कीटजन्य बीमारियाँ और मलेरिया जैसी बीमारियाँ बढ़ेंगी।
- जिससे जनसंख्या में और इससे संबंधित कई बदलाव आने वाली पीढ़ी की देखने होंगे।
| PDF Download Link |
| कक्षा 11 भूगोल के अन्य अध्याय के नोट्स | यहाँ से प्राप्त करें |