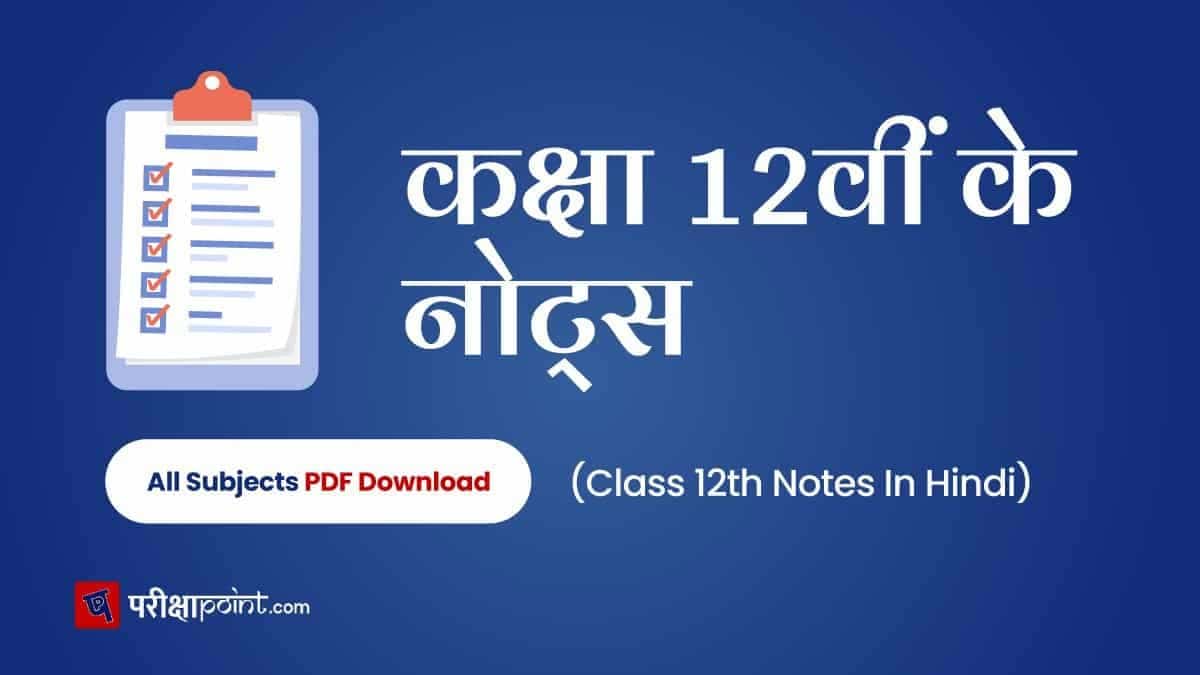इस लेख में छात्रों को एनसीईआरटी 12वीं कक्षा की इतिहास की पुस्तक-2 यानी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग- 2 के अध्याय- 5 यात्रियों के नज़रिए (समाज के बारे में उनकी समझ) के नोट्स दिए गए हैं। विद्यार्थी इन नोट्स के आधार पर अपनी परीक्षा की तैयारी को सुदृढ़ रूप प्रदान कर सकेंगे। छात्रों के लिए नोट्स बनाना सरल काम नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों का काम थोड़ा सरल करने के लिए हमने इस अध्याय के क्रमानुसार नोट्स तैयार कर दिए हैं। छात्र अध्याय- 5 इतिहास के नोट्स यहां से प्राप्त कर सकते हैं।
Class 12 History Book-2 Chapter-5 Notes In Hindi
आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से ये नोट्स फ्री में पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने के लिए इस पेज पर बने रहें और ऑफलाइन पढ़ने के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें। एक लिंक पर क्लिक कर आसानी से नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए ये नोट्स बेहद लाभकारी हैं। छात्र अब कम समय में अधिक तैयारी कर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे, यह अध्याय पीडीएफ के तौर पर भी डाउनलोड हो जाएगा।
अध्याय- 5 “यात्रियों के नज़रिए” (समाज के बारे में उनकी समझ)
| बोर्ड | सीबीएसई (CBSE) |
| पुस्तक स्रोत | एनसीईआरटी (NCERT) |
| कक्षा | बारहवीं (12वीं) |
| विषय | इतिहास |
| पाठ्यपुस्तक | भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग-2 |
| अध्याय नंबर | पाँच (5) |
| अध्याय का नाम | “यात्रियों के नज़रिए” (समाज के बारे में उनकी समझ) |
| केटेगरी | नोट्स |
| भाषा | हिंदी |
| माध्यम व प्रारूप | ऑनलाइन (लेख) ऑफलाइन (पीडीएफ) |
कक्षा- 12वीं
विषय- इतिहास
पुस्तक- भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग-2
अध्याय- 5 “यात्रियों के नज़रिए” (समाज के बारे में उनकी समझ)
अल-बिरुनी का यात्रा वृत्तांत (किताब-उल-हिन्द)
ख़्वारिज़्म से पंजाब तक
- अल-बिरुनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख़्वारिज़्म में 973 ई. में हुआ। यह जगह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अल-बिरुनी को फारसी, हिब्रू, संस्कृत जैसी अनेक भाषाओं का अच्छा ज्ञान था लेकिन उन्हें यूनानी भाषा नहीं आती थी।
- महमूद गजनवी ख़्वारिज़्म वियज के बाद अल-बिरुनी को बाकी विद्वानों के साथ गजनी ले आया। जिसके बाद उसने ब्राह्मण पुरिहितों तथा विद्वानों के साथ संस्कृत दर्शन और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। जिससे पता चलता है वह दार्शनिक विचारों वाला यात्री था।
- जब इस यात्री ने लिखना शुरू किया उस समय तक यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे।
किताब-उल-हिन्द
- अल-बिरुनी ने अपनी पुस्तक किताब-उल-हिन्द हिन्द की रचना सरल अरबी भाषा में की थी। जिसे उसने 80 अध्यायों में विभाजित किया था। जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति-रिवाजों एवं प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार-तौल और मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान इत्यादि जैसे अनेक विषयों को अपनी पुस्तक में शामिल किया है।
- अगर इस पुस्तक की शैली की बात की जाए, तो शुरुआत में एक प्रश्न होता था, उसके बाद संस्कृतवादी परंपराओं पर विस्तार से वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलनात्मक वर्णन।
- विद्वानों को लगता है कि इसकी पुस्तक ज्यामितीय संरचना में बनी हुई है इसलिए उसका झुकाव गणित की तरफ रहा होगा।
- इसको संस्कृत, पालि एवं प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवाद और रूपांतरण की भी जानकारी थी, जिनमें मुख्य रूप से दंत कथाओं, चिकित्सा और खगोल विज्ञान जैसी कृतियाँ शामिल थीं।
अल-बिरुनी का सामाजिक चित्रण और जाति व्यवस्था
- अल-बिरुनी ने उस समय के समाज का चित्रण किया है जब जाति व्यवस्था को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा था।
- अल-बिरुनी ने भारत की जाति प्रथा की तुलना अन्य देशों के साथ की है; जैसे कि फारस में चार घुड़सवार और शासक, भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित एवं चिकित्सक, खगोलशास्त्री और अन्य वैज्ञानिक साथ ही कई कृषक एवं शिल्पकार शामिल थे।
- अल-बिरुनी ने भारतीय समाज को समझने के लिए वेदों, पुराणों, भगवद्गीता, पतंजलि की कृतियों और मनुस्मृति का उपयोग स्त्रोत रूप में किया था। इसलिए उसके वृत्तांत का झुकाव संस्कृत ग्रंथों की तरफ अधिक लगता है।
- उसने अपनी पुस्तक में बताया है कि भारत में जाति-व्यवस्था के नियमों का पालन कठोरता के साथ नहीं होता था और अछूत लोग समाज से मिली पीड़ा को तो झेलते थे लेकिन उन्हें आर्थिक तंत्र में भी शामिल किया जाता था।
अल-बिरुनी का सामाजिक चित्रण और जाति व्यवस्था की सीमाएँ
- अल-बिरुनी के समय की संस्कृत भाषा अरबी भाषा से बहुत अलग थी इसलिए एक भाषा से दूसरे भाषा में किसी भी विचार को रूपांतरित या अनुवाद करना कठिन था।
- धर्मिक लोगों की मान्यताओं और रीति-रिवाजों में भिन्नता थी जिसे विस्तार से समझना मुश्किल था।
- उसने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि ब्राह्मणों के अभिमान को किसी तरह से ठेस न लगे और उसी आधार पर अपने वृत्तांत को एक विस्तृत रूप प्रदान किया।
- उसने भारत की समाज व्यवस्था को समझने के लिए वेदों, पुराणों, भगवद्गीता, पतंजलि की कृतियों और मनुस्मृति का उपयोग स्त्रोत रूप में किया था। इस प्रकार उसका वृत्तांत ब्राह्मणों द्वारा रचित ग्रंथों पर केंद्रित है।
इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत (रिह्ला)
विश्व-यात्री इब्न बतूता भारत में
- इब्न बतूता का जन्म तैंजियर के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवार में हुआ था। इनका परिवार इस्लाम और शरिया पर अपने विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध था।
- मोरक्को के निवासी इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत ‘रिह्ला’ को अरबी भाषा में लिखा है। भारत आने से पहले उसने मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमन और पूर्वी अफ्रीका के अनेक तटीय क्षत्रों की यात्रा की इसलिए इस यात्री को विश्व-यात्री के नाम से भी जाना जाता है।
- जब 1333 ई. में वह मध्य-एशिया से होते हुए भारत आया और दिल्ली पहुँचा तो मोहम्मद-बिन-तुगलक की प्रसिद्धि सुनकर, कला तथा साहित्य के संरक्षक के रूप उनके दरबार में पहुँचा जिसके बाद सुल्तान ने प्रभावित होकर उसे अपना न्यायाधिस (काजी) बना लिया। सुल्तान ने 1342 ई. में उसे मंगोल के राजा के पास दूत के रूप में भी भेजा था।
- इस यात्री को मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में 40 दिन और सिंध से दिल्ली की यात्रा करने में कम से कम 50 दिन का समय लगा।
- इसने दिल्ली में काजी के पद पर रहते हुए अनेक विदेशी यात्राएँ पूरी की। सबसे पहले वह मध्य-भारत और मालाबार से होते हुए मालदीव पहुँचा, जहाँ लहभग 18 महीने तक न्यायाधिस (काजी) के पद पर रहा।
- उसने श्रीलंका, चीन, असम और बंगाल की भी यात्रा की। इस तरह से यह एक हठीला यात्री होने के साथ-साथ जिज्ञासु भी था।
विश्व-यात्री इब्न बतूता का भरतीय समाज चित्रण
- इसने अपनी पुस्तक में बताया है कि सल्तनतकाल में सती प्रथा और दास प्रथा जैसी व्यवस्थाएँ भी समाज में चलन में थी। दास प्रथा के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा है कि बाजार में दासों को वस्तुओं की तरह खरीदा-बेचा जाता था साथ ही उपहार में वस्तु के स्थान पर दास दिए जाते थे।
- इब्न बतूता ने भी सुल्तान मोहम्मद-बिन-तुगलक को उपहार देने के लिए घोड़ा, ऊँट और दास खरीदे थे। उस समय महिलाओं को भी दासी बनाया जाता था जोकि संगीत और गाना गाने में विशेषता रूप से माहिर हुआ करती थीं।
- इब्न बतूता ने बताया है कि दास पालकी और डोली में महिला या पुरुष को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के साथ-साथ घरेलू कार्य भी करते थे लेकिन उन्हें मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। अमिर लोग अपने कई कार्यों पर नजर रखने के लिए दसियों को चुनते थे।
- इब्न बतूता ने शहरी व्यापार के बारे में बताते हुए कहा है कि दिल्ली सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर था। दौलताबाद जिसे आज महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है वह भी उस समय दिल्ली जैसा ही था।
- रिह्ला में बताया गया है कि अधिकतर बाजारों में एक मस्जिद और एक मंदिर जरूर होता था। ये बाजार व्यापार विनिमय ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विनिमय के लिए मुख्य स्थान हुआ करते थे। शहरों को अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गाँवों से प्राप्त होता था।
- उस समय भारतीय कपड़ों मुख्यतः सूती वस्त्र, महीन मलमल, रेशम, साटन जैसे कपड़ों के साथ कच्चे माल की माँग मध्य और दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे ज़्यादा थी। ऐसे में उस दौरान व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए कई व्यापारिक मार्गों पर व्यापारियों के लिए विश्राम घर और सराए बनाए गए।
- इब्न बतूता ने अपने किताब में उस समय की डाक व्यवस्था को कुशल बताते हुए कहा है गुप्तचरों का संदेश सुल्तान तक पहुँचाने में सिर्फ पाँच दिन का समय लगता था।
- उसने अपनी पुस्तक में भारत में उगाई जाने वाली वनस्पति उपज का विस्तृत वर्णन किया है, जिसमें मुख्य रूप से मानव सिर जैसे गिरिदार फल यानी नारियल और पान इत्यादि का जिक्र किया है।
बाहरी यात्रियों का आगमन
- लगभग 1400-1800 के बीच बहुत से यात्रियों ने अल-बिरुनी और इब्न बतूता के पदचिह्नों पर चलते हुए अपनी यात्रा वृत्तांत को फारसी भाषा में तैयार किया। जिनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखक अब्दुर रज्जाक है जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की। फिर महमूद वली बल्खी ने 1620 के दशक में और शेख अली हाजिन ने 1740 के दशक में भारत यात्रा की।
- जहाँ फ्रांसीसी जौहरी ज्यां बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने छः बार भारत की यात्रा की वहीं इतालवी चिकित्सक मनूची जैसे कई ऐसे भी व्यक्ति हुए जो भारत से प्रभावित होकर हमेशा के लिए यहीं बस गए।
फ्रांस्वा बर्नियर का यात्रा वृत्तांत (ट्रैवल्स इन द मुगल एंपायर)
- फ्रांस्वा बर्नियर उन विदेशी यात्रियों में शामिल था जो 1600 ई. के बाद भारत आए। यह यात्री होने के साथ-साथ इतिहासकार, दार्शनिक, चिकित्सक और राजनीतिज्ञ की श्रेणी में भी शामिल किया जाता है।
- इसका वृत्तांत तुलनात्मक था। वह जो भी भारत में देखता था उन स्थितियों/विचारों की तुलना यूरोपीय स्थितियों/विचारों से करता था। इसने अपनी पुस्तक फ्रांस के राजा लुई XIV को दे दिया।
- इसके यात्रा वृत्तांत का प्रकाश फ्रांस में 1670-71 ई. में हुआ। अपनी पुस्तक में इसने यूरोप के मुकाबले भारत की स्थिति को दयनीय बताया है।
- बर्नियर ने अपनी पुस्तक ‘ट्रैवल्स इन द मुगल एंपायर’ में मुगल काल के इतिहास का वैश्विक रूप दर्शाया है। यह पुस्तक विस्तृत अध्ययन और आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है।
- भारत के सामाजिक परिदृश्य को दर्शाने के लिए इसने सल्तनतकालीन और मुगलकालीन सामाजिक भेदभाव को दिखाया है जिसके लिए मुख्य केंद्र महिलाओं को बनाया है।
- इसने ‘सती प्रथा’ के बारे में कहा है कि उस समय कुछ महिलाएँ सामाजिक दबाव में अपने पति के मरने के बाद मृत्यु को अपना लेती थीं, तो कुछ अपनी इच्छा से मर जाती थीं। वही स्त्रियाँ आर्थिक, कृषि, व्यापारिक जैसे कार्यों में भी हिस्सा लेती थीं। उस समय उच्च वर्ग की स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि स्त्रियाँ सिर्फ घरों तक सीमित नहीं थीं।
- बर्नियर ने भारत की आर्थिक स्थिति ठीक न होने कारण भू-स्वामित्व की कमी को बताया है। क्योंकि भूमि पर बादशाहों का अधिकार होता था लेकिन ये राज्य और जनता दोनों के लिए किसी प्रकार से लाभकारी नहीं था।
- गरीब भारतीय जनता पर शक्तिशाली शासकों और धनी वर्ग के लोगों का अधिकार होता था। उस समय अमीर और गरीब सिर्फ दो ही वर्ग हुआ करते थे, मध्य-वर्ग अभी उत्पन्न नहीं हुआ था।
- मुगल काल के शहरों को बर्नियर ने ‘शिविर नगर’ कहा जोकि राजकीय शिविर पर निर्भर थे।
- उस समय सभी प्रकार के विभिन्न नगर थे; जैस कि व्यापारिक नगर, बंगरगाह नगर आदि और व्यापारी अपनी जाति व्यवसाय क्षेत्र के अनुसार संगठित होते थे।
- इस पुस्तक में बताया गया है अहमदाबाद (गुजरात) में महाजनों का प्रतिनिधित्व व्यापारी समुदाय का मुखिया यानी ‘नगर सेठ’ करता था। इन व्यवसायियों में अध्यापक, चिकित्सक, अधिवक्ता, संगीतकार, चित्रकार, वास्तुविद और लेखक इत्यादि शामिल थे। कुछ लोग बाजारों में सेवा करके अपना जीवन बिताते थे।
बर्नियर के विचारों का खंडन
- कई जगह पर बर्नियर के विचारों में विरोधाभास साफ-साफ दिखाई देता है। एक तरफ तो उसने यह बताया कि शिल्पकारों द्वारा अपने उत्पादन को बेहतर बनाने का प्रयास नहीं किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा कि संपूर्ण विश्व से अधिक मात्रा में कीमती धातुएँ भारत आती थीं क्योंकि उत्पादों का निर्यात सोने और चाँदी के बदले होता था।
- इसकी पुस्तक में भू-संबंधित विवाद भी देखने को मिलते हैं। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने भू-राजस्व को राजस्व का पारिश्रमिक बताया है जिसे भूमि लगान के रूप में नहीं बल्कि शासक द्वारा अपनी जनता की रक्षा के बदले में लिया जाता था।
- बर्नियर ने ग्रामीण समुदाय के बारे में जो चित्र प्रस्तुत किया है वो भी विवादित नजर आता है।
- फिर भी फ्रांस्वा बर्नियर के वृत्तांत और विचारों को पूरी तरह से नकारा नहीं गया। जैसे कि मांटेस्क्यू ने बर्नियर के वृत्तांतों का प्रयोग प्राच्य निरंकुशतावाद के सिद्धांत को विस्तृत रूप देने के लिए किया।
- वहीं 19वीं शताब्दी में काल मार्क्स ने बर्नियर के वृत्तांत और विचारों का उपयोग ‘एशियायी-उत्पादन’ शैली के सिद्धांत को विस्तृत रूप प्रदान करने के लिए किया था।
समयावधि अनुसार घटनाक्रम
वृत्तांत छोड़ने वाले यात्रियों का वर्णन
| क्रम संख्या | काल | घटना |
| 1. | दसवी-ग्यारहवीं शताब्दियाँ 973-1048 | मोहम्मद इन अहमद अबू रेहान अल बिरूनी (उज़्बेकिस्तान से) |
| 2. | तेरहवीं शताब्दी 1254-1823 | मार्को पोलो (इटली से) |
| 3. | चौदहवीं शताब्दी 1304-77 | इब्न बतूता (मोरक्को से) |
| 4. | पंद्रहवीं शताब्दी 1413-82 | अब्द अल-रज्जाक कमाल अल-दिन इन इस्हाक़ अल-समरकंदी (समरकंद से) |
| 5. | 1466-72 (भारत में बिताए वर्ष) | अफानासी निकितिच निकितिन (पंद्रहवीं शताब्दी, रूस से) |
| 6. | सोलहवीं शताब्दी 1562 (मृत्यु का वर्ष) | दूरते बारबोसा, मृत्यु 1521 (पुर्तगाल से) |
| 7. | 1562 (मृत्यु का वर्ष) | सयदी अली रेइस (तुर्की से) |
| 8. | 1536-1600 | अंतोनियो मानसेरेते (स्पेन से) |
| 9. | सत्रहवीं शताब्दी 1626-31 (भारत में बिताए वर्ष) | महमूद वली बलखी (बल्ख से) |
| 10. | 1600-67 | पीटर मुंडी (इंग्लैंड से) |
| 11. | 1605-89 | ज्यां बैप्टिस्ट तैवर्नियर (फ्रांस से) |
| 12. | 1620-88 | फ्रांस्वा बर्नियर (फ्रांस से) |
| कक्षा 12 इतिहास के अन्य अध्याय के नोट्स | यहाँ से प्राप्त करें |