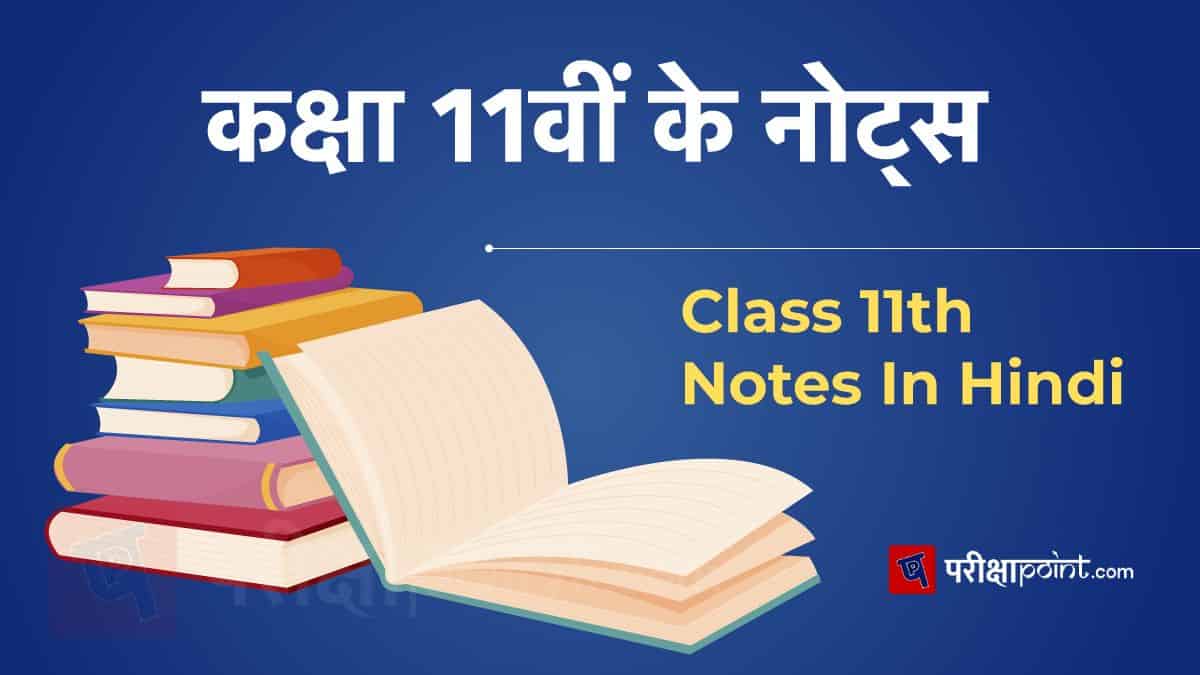इस लेख में छात्रों को एनसीईआरटी 11वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक-1 यानी “राजनीतिक सिद्धांत” के अध्याय- 3 “समानता” के नोट्स दिए गए हैं। विद्यार्थी इन नोट्स के आधार पर अपनी परीक्षा की तैयारी को सुदृढ़ रूप प्रदान कर सकेंगे। छात्रों के लिए नोट्स बनाना सरल काम नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों का काम थोड़ा सरल करने के लिए हमने इस अध्याय के क्रमानुसार नोट्स तैयार कर दिए हैं। छात्र अध्याय 3 राजनीति विज्ञान के नोट्स यहां से प्राप्त कर सकते हैं।
Class 11 Political Science Book-1 Chapter-3 Notes In Hindi
आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दो ही तरह से ये नोट्स फ्री में पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने के लिए इस पेज पर बने रहें और ऑफलाइन पढ़ने के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें। एक लिंक पर क्लिक कर आसानी से नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए ये नोट्स बेहद लाभकारी हैं। छात्र अब कम समय में अधिक तैयारी कर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे, यह अध्याय पीडीएफ के तौर पर भी डाउनलोड हो जाएगा।
अध्याय- 3 “समानता”
| बोर्ड | सीबीएसई (CBSE) |
| पुस्तक स्रोत | एनसीईआरटी (NCERT) |
| कक्षा | ग्यारहवीं (11वीं) |
| विषय | राजनीति विज्ञान |
| पाठ्यपुस्तक | राजनीतिक सिद्धांत |
| अध्याय नंबर | तीन (3) |
| अध्याय का नाम | समानता |
| केटेगरी | नोट्स |
| भाषा | हिंदी |
| माध्यम व प्रारूप | ऑनलाइन (लेख) ऑफलाइन (पीडीएफ) |
कक्षा- 11वीं
विषय- राजनीति विज्ञान
पुस्तक- राजनीतिक सिद्धांत
अध्याय-3 “समानता”
समानता की महत्वता
- समानता मानव-समाज में कई वर्षों से विद्यमान है, जो प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व को सर्वोपरि रखता है।
- इसके अंतर्गत ऐसी विशिष्टाओं पर जोर दिया जाता है, कि मनुष्य कई विविधताओं (जैसे, रंग, वर्ण, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के आधार पर) के बाद भी समान है।
- 18वीं सदी में हुई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा फ्रांसीसियों का नारा बन गया था, यह मांग 19वीं सदी में एशिया, अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलनों के दौरान भी उठी।
- आज के समय में समानता को विभिन्न राज्यों की सरकारों ने अपने संविधान का हिस्सा बनाया है। लेकिन इस सब के बाद भी हमारे देश में भी कुछ स्थानों पर असमानता देखी जा सकती है।
- समानता का महत्व सभी जानते हैं, लेकिन हमारे समाज में ही बड़े स्तर पर असमानता लगभग हर तरफ देखी जा सकती है।
- क्या समानता प्राप्ति करके मनुष्य लोगों के मध्य व्याप्त सभी प्रकार की भिन्नताओं को मिटाना चाहता है?क्या सभी लोगों में पूर्ण समानता संभव है?
समानता क्या है?
- मानवता के पहलू से देखा जाए तो, समानता का अर्थ, सभी मनुष्यों को बराबर का सम्मान और हक दिया जाने से है।
- समाज अपने सदस्यों से हमेशा एक समान बर्ताव नहीं कर सकता, कार्यों के विभाजन के आधार पर यह बर्ताव भिन्न होता है।
- जैसे देश के प्रधानमंत्री को दिया जाने वाला सरकारी दर्जा, समानता की धारणा के अनुकूल ही है। इसके विपरीत नागरिकों के साथ समाज में व्याप्त बुनियादी असमानताऐं अन्यायपूर्ण लगती हैं।
- मनुष्य के रंग, लिंग, धर्म, जाति, जन्मस्थान आदि के आधार पर असमान बर्ताव को अक्सर नकारात्मक रूप से देखा जाता है, क्योंकि इन सभी कारकों पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है।
- समानता का अर्थ यह नहीं हो सकता की किसी भी प्रकार का भेद ही न हो, समानता का सरल अर्थ है, कि हमारे साथ होने वाले बर्ताव पर हमारे रंग, लिंग, वर्ग, जाति आदि का असर न पड़े।
अवसरों की समानता
- संबंधित देश का हर नागरिक अपने विकास के लिए, समान अधिकारों और अवसरों का हकदार है, जो हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं, जिसके कारण उनके सफल होने की संभावनाएं कम या अधिक भी हो सकती हैं।
- समाज में विशेषाधिकार का अभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बुनियादी जरूरतों को समान रूप से न उपलब्ध करा पाने वाला समाज अन्यायपूर्ण और असमान है।
- प्राकृतिक असमानताएं- इसके अंतर्गत व्यक्ति की जन्मगत या योग्यता के आधार पर विशिष्टा को सम्मिलित किया जाता है।
- सामाजिक असमानताएं– इन असमानताओं में समाज द्वारा जनित असमानताओं को रखा जाता है।
- इन दोनों में भेद का मुख्य कारण यह है, ताकि अन्यायपूर्ण और न्यायपूर्ण असमानता के बीच भेद स्पष्ट हो सके।
- लेकिन, प्राकृतिक रूप से भिन्न बर्ताव करने वालों को जन्मजात ही उस बर्ताव के साथ ढाल दिया जाता है, जैसे महिलाओं के लिए ‘अबला’ शब्द का प्रयोग होना, और उन्हें समानता के अधिकार से वंचित कर देना जैसी समस्याएं इस स्थिति में उत्पन्न होती हैं।
- प्राकृतिक और सामाजिक असमानता में भेद कर किसी कानून का निर्धारण करना कठिन होता है।
समानता के तीन आयाम
- राजनीतिक समानता-
- लोकतंत्र में देश के सभी नागरिकों को मताधिकार, कहीं आने-जाने, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त होता है।
- इन अधिकारों से नागरिक लोकतंत्र में हिस्सा ले सकते हैं, सरकार का चुनाव कर सकते हैं।
- ये औपचारिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं।
- राजनीतिक समानता समतावादी समाज के गठन के लिए महत्वपूर्ण है।
- सामाजिक समानता-
- राजनीतिक समानता के द्वारा समाज में अवसरों की समानता को नागरिकों तक पहुंचाया जाता है।
- समाज में नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देना भी आवश्यक है।
- समान अवसरों के अभाव में प्रतिभा का खजाना बेकार हो जाता है।
- समाज में व्याप्त रीति-रिवाजों के कारण नागरिकों को समान अवसर मिलने में समस्या होती है, जैसे महिलाओं को उत्तराधिकार का समान अधिकार न मिलना।
शहरी भारत में उच्च शिक्षा में जातिगत समुदायों में असमानता
| जातिगत समुदाय | स्नातक लोगों की संख्या / 1000 में |
| अनुसूचित जाति | 47 |
| मुस्लिम | 67 |
| हिन्दू (अन्य पिछड़ा वर्ग) | 86 |
| अनुसूचित जनजाति | 109 |
| ईसाई | 237 |
| सिख | 250 |
| हिन्दू (उच्च जातियाँ) | 253 |
| अन्य धार्मिक समुदाय | 315 |
| अखिल भारतीय औसत | 155 |
- आर्थिक समानता–
- ऐसा समाज जहां धन-संपत्ति के आधार पर भिन्नता पाई जाए, आर्थिक समानता की आवश्यकता वहां होती है।
- आर्थिक असमानता को जानने के लिए अति धनवान और अति निर्धन व्यक्ति के बीच का अंतर जानना, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या का आंकलन कर पता की जा सकती है।
- समान अवसर प्रदान कर लोगों को उनके हालात सुधारने के लिए उचित मौका दिया जाता है, जो प्रतिभा के धनी हैं।
- वे असमानताएं हानिकारक हैं जहां गरीब तबका गरीब बना हुआ है, और अमीर, और भी अमीर। इससे समुदायों में आक्रोश जन्म लेता है।
राजनीतिक विचारधाराएं
- मार्क्सवादी विचारधारा–
- मार्क्स जो 19वीं सदी के विचारक रहे हैं, ने बताया कि समाज में व्याप्त असमानता का बुनियादी कारण है, देश के संसाधनों का निजी हाथों में स्वामित्व।
- जो अमीर वर्ग को राजनीतिक शक्ति भी प्रदान करता है। यह ताकतें राजनीतिक निर्णयों को भी प्रभावित करती हैं।
- आर्थिक असमानता के परिणामस्वरूप सामाजिक असमानताओं का जन्म होता है, यही करण है कि सामाजिक समानता को बनाने के लिए समान अवसर की उपलब्धता के साथ-साथ, संसाधनों और संपत्ति पर जनता का नियंत्रण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- उदारवादी विचारधारा–
- उदारवादियों के अनुसार संसाधनों का वितरण प्रतिस्पर्धा के आधार पर होना उचित है।
- उनके अनुसार संसाधनों का समान वितरण करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए।
- संसाधनों के वितरण के लिए की जानें वाली प्रतिस्पर्धाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, जिससे असमानताएं अधिक न हों।
- इनका मत है कि नौकरियों और पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए कराई जाने वाली परीक्षाएं ही न्यायोचित सिद्धांत है।
- राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं हैं, राजनीतिक समानता लोकतंत्र द्वारा हासिल की जा सकती है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए अन्य रणनीतियाँ तलाशनी होंगी।
समानता को बढ़ावा कैसे दें?
- औपचारिक समानता द्वारा–
- सभी औपचारिक विशेषाधिकार समाप्त करके समानता स्थापित की जाती है।
- बुनियादी असमानताओं को कानूनों और रीति-रिवाजों के जरिए महत्वपूर्ण बना दिया गया है, जिससे समाज के कुछ वर्गों को अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रखा जाता है।
- भारत में विद्यमान जाति व्यवस्था, निचले वर्ग के लोगों को केवल शारीरिक श्रम करने की ही अनुमति देती है।
- इसके लिए सभी विशेषाधिकारों को समाप्त करना अनिवार्य है, जिसको सरकार एवं कानून ही संरक्षण प्रदान करता है।
- भारत के संविधान छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन करता है, आज के दौर की लोकतान्त्रिक सरकारें समानता के सिद्धांत का स्वीकार करती है, और नागरिकों के साथ समान बर्ताव के कानून के हक में है।
- विभेदक बर्ताव से समानता–
- कानून के समक्ष समानता ही पर्याप्त नहीं है, कुछ लोगों के बीच में अंतर के द्वारा समानता का मार्ग प्रशस्त होता है।
- जैसे सार्वजनिक स्थानों पर विकलांग जनों के लिए ढलान वाला रास्ता बनाकर।
- अवसरों को समान रूप से नागरिकों तक पहुँचने के लिए कुछ देशों में सकारात्मक कार्रवाई की नीति अपनाई है।
- सकारात्मक कारवाई– इसके अंतर्गत वंचित छात्रों के लिए छात्रवृति, नौकरी और शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था की नीतियाँ शामिल हैं। भारत में इसे कोटा या आरक्षण कहा जाता है।
- विशेष उपायों के जरिए इन वंचित समुदायों को वर्तमान पिछड़ेपन से उभारा जा सके।
- सकारात्मक विभेदीकरण– आरक्षण के आलोचकों का मानना है कि इससे समानता के सिद्धांत को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है, और समाज के अन्य वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।
- आरक्षण उनकी नजर में भेदभाव का ही जरिया है। ये सिद्धांतकार मानते हैं कि ऐसे किसी भी व्यवहार को समाप्त किया जाना चाहिए जो समाज को विभाजित करता है।
आरक्षण की आवश्यकता
- उचित प्रतिस्पर्धा के द्वारा व्यक्ति का किसी शैक्षिक संस्था या नौकरी में प्रवेश होना चाहिए।
- जो शिक्षार्थी अपने परिवार में पहली वह पीढ़ी है जो शिक्षित हैं, ये छात्र अपनी जरूरतों के आधार पर सक्षम वर्ग से भिन्न होते हैं।
- इन वर्गों को विशेष सहायता प्रदान करने के लिए राज्य को नीतियाँ निर्धारित करनी चाहिए।
- भारत में वंचित वर्गों के लिए बेहद कम कार्य किए गए हैं।
- स्कूली शिक्षा के स्तर पर व्याप्त असमानताएं हैं, जिसके कारण वे शिक्षा से वंचित और रोजगार से कोसो दूर हैं।
- ऐसे ही छात्र जब आगे जाकर प्रवेश परीक्षा में बैठतें हैं, तब शिक्षा का उच्च स्तर न मिल पाने के कारण ये अन्य सक्षम छात्रों से पीछे रह जाते हैं।
- यही कारण है कि यह वर्ग समानता के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं जीत सकते।
- इन्हीं कारणों से आज सिद्धांतकारों ने भी इस बात पर सहमति जताई है। राज्य द्वारा अपनाई गई नीतियों को लेकर ही विवाद उत्पन्न होते हैं। क्या सरकार की नीतियाँ समानता के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाईं हैं।
- नारीवादी आंदोलन और समानता– महिलाओं ने 19वीं सदी में आंदोलन कर पुरुषों के समान अधिकारों की मांग की, जिसके साथ ही अब महिलाओं के लिए नौकरियों या अन्य स्थानों पर विशेषाधिकारों (जैसे मातृत्व अवकाश) की मांग भी तेज हो गई।
- कई बार विशेष अधिकारों के माध्यम से समानता को हासिल किया जा सकता है, जिससे सम्पूर्ण समाज को भी यह न्यायपूर्ण लग सके, और यह शोषण या वर्चस्व का जन्मदाता न बन जाए।
| PDF Download Link |
| कक्षा 11 राजनीति विज्ञान के अन्य अध्याय के नोट्स | यहाँ से प्राप्त करें |