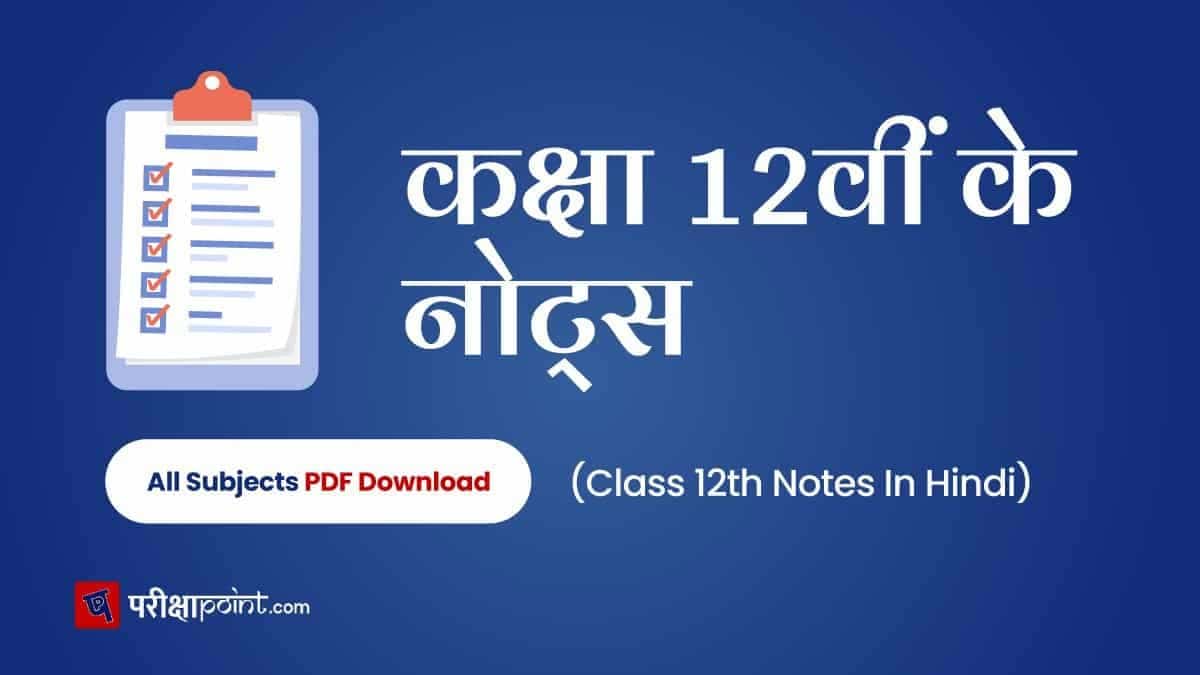इस लेख में छात्रों को एनसीईआरटी 12वीं कक्षा की इतिहास की पुस्तक-1 यानी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग- 1 के अध्याय- 4 विचारक, विश्वास और इमारतें (सांस्कृतिक विकास) के नोट्स दिए गए हैं। विद्यार्थी इन नोट्स के आधार पर अपनी परीक्षा की तैयारी को सुदृढ़ रूप प्रदान कर सकेंगे। छात्रों के लिए नोट्स बनाना सरल काम नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों का काम थोड़ा सरल करने के लिए हमने इस अध्याय के क्रमानुसार नोट्स तैयार कर दिए हैं। छात्र अध्याय- 4 इतिहास के नोट्स यहां से प्राप्त कर सकते हैं।
Class 12 History Book-1 Chapter-4 Notes In Hindi
आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दो ही तरह से ये नोट्स फ्री में पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने के लिए इस पेज पर बने रहें और ऑफलाइन पढ़ने के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें। एक लिंक पर क्लिक कर आसानी से नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए ये नोट्स बेहद लाभकारी हैं। छात्र अब कम समय में अधिक तैयारी कर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे, यह अध्याय पीडीएफ के तौर पर भी डाउनलोड हो जाएगा।
अध्याय- 4 “विचारक, विश्वास और इमारतें” (सांस्कृतिक विकास)
| बोर्ड | सीबीएसई (CBSE) |
| पुस्तक स्रोत | एनसीईआरटी (NCERT) |
| कक्षा | बारहवीं (12वीं) |
| विषय | इतिहास |
| पाठ्यपुस्तक | भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग-1 |
| अध्याय नंबर | चार (4) |
| अध्याय का नाम | “विचारक, विश्वास और इमारतें” (सांस्कृतिक विकास) |
| केटेगरी | नोट्स |
| भाषा | हिंदी |
| माध्यम व प्रारूप | ऑनलाइन (लेख) ऑफलाइन (पीडीएफ) |
कक्षा- 12वीं
विषय- इतिहास
पुस्तक- भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग-1
अध्याय- 4 “विचारक, विश्वास और इमारतें” (सांस्कृतिक विकास)
साँची की एक झलक
- प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत साँची अंखेड़ा की इमारते हैं जो भोपाल राज्य में हैं। इसके रखरखाव के लिए शासकों, शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तानजहाँ बेगम ने धन अनुदान दिया।
- ‘जॉन मार्शल’ ने साँची पर अनेक पुस्तकें लिखीं जिसके विभिन्न खंडों के प्रकाशन के लिए ‘सुल्तानजहाँ बेगम’ ने अनुदान दिया।
बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि
वैदिक धर्म
- वैदिक धर्म की शुरुआत 1500 से 1000 ईसा. पूर्व. के आस-पास मानी जाती है। वैदिक काल के बारे में जानने के लिए ऋग्वेद को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस ग्रंथ में इन्द्र, अग्नि और सोम को उस समय का मुख्य देवता माना गया है।
- वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था, इस धर्म के लोग उपासना करने के लिए यज्ञ किया करते थे। राजाओं और सरदारों द्वारा क्रमशः राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे।
- ब्राह्मण धर्म में जन्म-मृत्यु और पुनर्जन्म से जुड़ी अवधारणों पर ज़्यादा बल दिया गया।
जैन धर्म
- जब ब्राह्मण धर्म के कर्मकांड संबंधी सिद्धांत अधिक जटिल हो गए तब इसका खंडन करने के लिए जैन संप्रदाय का विकास हुआ।
- वर्धमान महावीर के साथ 24 तीर्थकरों ने मिलकर जैन धर्म के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया।
- इस धर्म के मुताबिक पूरा संसार प्राणवान है। पत्थर, पहाड़ और जल में भी जीवन होता है। अहिंसा को अपनाना ही जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है। इसमें सबसे अधिक कर्म करने पर बल दिया गया है क्योंकि जैन धर्म के के अनुसार मुक्ति अच्छे कर्म करने से प्राप्त होती है।
- हत्या न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संचयन करना ये पाँच व्रत पुरुषों और स्त्रियों के लिए बताए गए जिन्हें साधु और साध्वी कहा जाता था।
- जैन धर्म के सिद्धांत इतने सरल थे कि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से अपने जीवन में उतार सकता था। यही कारण है कि जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी अनेक साहित्यों में विशेष योगदान दिया। उसके बाद यह धर्म भारत के अनेक हिस्सों में फैल गया।
बौद्ध धर्म
- जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म का उदय हुआ लेकिन बौद्ध धर्म में कर्मवाद को अपनाकर भौतिक्तावाद का त्याग किया गया।
- महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शक्य कबीले के एक सरदार के घर में जन्म होने के कारण आरंभ में इन्हें सभी सुख-सुविधाएँ प्राप्त हुईं।
- जब वो एक दिन घर से बाहर शहर घूमने गए, तो रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव को देखकर अत्यंत दुखी हो गए। उसके बाद जीवन के सत्य को जानने के लिए उन्होंने घर त्याग करने का मन बना लिया।
- घर त्यागने के बाद सत्य की खोज के लिए उन्हें कठोर उपासना करनी पड़ी, जिसके बाद उनकी स्थिति बेजान मनुष्य जैसी हो गई थी।
- जिस बुद्ध को प्रारंभिक मूर्तिकारों ने मनुष्य रूप के स्थान पर प्रतीकों के रूप में दर्शाया है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। स्तूप महापरिनिर्वाण और धर्मचक्र बुद्ध के प्रथम उपदेश को दर्शाता है।
- बुद्ध कहते हैं कि संसार नश्वर है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी और शाश्वत नहीं है, यह आत्मयविहीन है। संसार दुखों से भरा हुआ है लेकिन मध्यम-मार्ग पर चलकर व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। राजाओं और धनवान लोगों को दयावान और आचारवान होना चाहिए। व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश में बदलाव किया जा सकता है।
- इस धर्म में जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण हेतु सम्यक क्रम की कल्पना की गई है। ये सभी बुद्ध की शिक्षाएँ हैं जोकि सुत्तपिटक की कहानियों पर आधारित हैं।
बुद्ध के अनुयायी
- महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों आनंद और उपाली के साथ मिलकर एक संघ की स्थापना की, जिसके गुरु महात्मा बुद्ध थे। संघ में रहने वाले सभी व्यक्ति बुद्ध की तरह ही सादा जीवन व्यतीत करते थे।
- पहले संघ में सिर्फ पुरुष ही शामिल हो सकते थे लेकिन बाद में शिष्य आनंद ने बुद्ध की आज्ञा पाकर महिलाओं को भी संघ में आने की अनुमति प्रदान की। संघ में सभी को एक समान माना जाता था इसलिए इसमें राजा, दास, गृहपति, कर्मकार से लेकर शिल्पकार भी शामिल हुए।
- संघ में शामिल कुछ महिलाएँ धम्म की उपदेशिकाएँ बनीं, तो कुछ महिलाएँ बदलते समय के साथ थेरी बनी। दरअसल थेरी उन महिलाओं को कहा जाता था जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो।
- बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ही तेजी से फैला और जो लोग उस समय के धार्मिक सिद्धांतों या प्रथाओं से दुखी थे वे इस धर्म की ओर सबसे अधिक आकर्षित हुए।
- पहली सदी के बाद बौद्ध सिद्धांतों को लेकर अनुयायियों में विरोधाभाष उत्पन्न हो गया जिसके बाद बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान शाखाओं में हो गया।
हिंदू धर्म
- मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं रही। हिंदू धर्म के अंतर्गत वैष्णव (भगवान विष्णु के भक्त) और शैव (भगवान शिव के भक्त) मुख्य दो संप्रदाय हुए। इस धर्म में यज्ञ और बलि का स्थान प्रेम और भक्ति ने ले लिया।
- हिंदू धर्म में जिन देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं उनकी मुद्राएँ प्राचीन कहानियों पर आश्रित होती थीं।
- उस समय महिलाओं और शूद्रों को संस्कृत श्लोकों में लिखी गई प्राचीन कहानियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसलिए इन कहानियों को तेज आवाज में पढ़ा जाता था ताकि वे लोग भी इन कहानियों को जान सकें।
इमारतों की संरचना और स्थापत्य कला
प्राचीन समय में लोग कुछ जगहों को सबसे अधिक पवित्र मानते थे जिसमें कुछ और चट्टानें मुख्य रूप से शामिल थीं। कुछ जगहों पे छोटी-सी वेदी भी बनी रहती थी जिन्हें कभी-कभी चैत्य भी कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों का जिक्र मिलता है जिसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है।
स्तूप
- बुद्ध से जुड़े अवशेषों; जैसे कि- आस्तियां, उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, उनके नाखून आदि को बुद्ध से जुड़े पवित्र जगहों पर गोलार्ध मिट्टी के टीले के नीचे दबा दिया जाता था। गोलार्ध संरचना में बनाए गए इन्हीं टीलों को स्तूप कहा जाता था।
- स्तूप मुख्य रूप से लुम्बिनी (बुद्ध के जन्म स्थल), बोधगया (ज्ञान प्राप्ति), सारनाथ (उपदेश), कुशीनगर (निब्बान प्राप्त किया) जैसी जगहों पर बनाए गए।
- बौद्ध ग्रंथ “अशोकावदान” में बताया गया है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को हर एक महत्वपूर्ण शहर में बँटवाया और उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया।
- भरहुत, साँची और सारनाथ जैसे कई स्थानों पर ईसा पूर्व दूसरी सदी तक स्तूप बन चुके थे।
- स्तूपों निर्माण और उनकी सजावट के बारे में जानकरी उनकी वेदिकाओं, स्तंभों पर मिले अभिलेखों में दान की चर्चा से प्राप्त होती है। ये दान सातवाहन शासकों, व्यापारियों और शिल्पकारों द्वारा दिए जाते थे। स्तूप पहले गोल मिट्टी के टीले जैसे होते थे जिन्हें अंड कहा जाता था। बाद में इन्हें चौकोर और गोल आकार के संतुलन में जटिल रूप दे दिया गया।
- अंड के ऊपर एक हार्मिका होती थी और हार्मिका से एक मस्तूल निकलता था, जिसे यष्टि कहा जाता था। स्तूप के चारों तरफ एक वेदिका होती थी, जोकि एक पवित्र स्थल था।
- स्तूप में ताखों और मूर्तियाँ उत्कीर्ण करने की कला अमरावती स्तूप में देखने को मिलती है।
साँची का स्तूप
- साँची का स्तूप भोपाल से 20 मील उत्तर-पूर्व दिशा में एक पहाड़ी पर बना है। यहाँ का प्राचीन तोरणद्वार और बुद्ध की मूर्ति लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
- जब सन् 1818 में विद्वानों के खोजबीन शुरू की तो उस दौरान उन्हें तीन तोरणद्वार खड़े मिले लेकिन चौथा वहीं गिरा हुआ था। अंग्रेज इसे अपने साथ पेरिस/लंदन ले जाना चाहते थे लेकिन यह भारत का सौभाग्य था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी ये स्तूप वहीं बना हुआ है।
- इतिहासकारों का कहना है कि साँची के स्तूप में कई कहानियों को चित्र से रूप में अंकित किया गया है। जिसमें से एक दृश्य ‘वेसांतर जातक’ से लिया गया है। इस कहानी के अनुसार एक दानी राजकुमार अपना सब कुछ ब्राह्मण को दान देकर खुद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वनवासी हो जाता है।
- साँची के स्तूप की संरचना में सबसे अधिक मूर्ति कला का प्रभाव नजर आता है; जैसे कि- स्तूप के तोरण द्वार पर बनी शालभंजिक के रूप में सुंदर स्त्री की मूर्ति।
- इस स्तूप में घोड़े, बंदर, हाथी, गाय, साँप और बैल जैसे कई जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है।
- इन प्रतीकों के माध्यम से कहीं-कहीं बुद्ध की माँ ‘माया’ और सौभाग्य की देवी ‘गजलक्ष्मी’ को भी दिखाया गया है। वहीं यहाँ चक्र को सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक माना गया है, तो पेड़ को ज्ञान प्राप्ति के रूप में दर्शाया गया है। इस स्तूप में वेसांतर जैसी जातक कथाओं के चित्रांकन भी देखने को मिलते हैं।
अमरावती का स्तूप
- एक स्थानीय राजा मंदिर का निर्माण 1796 ई. में कराना कहते थे, उसी समय उन्हें अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। उन्हें लगा वहाँ कोई खजाना है, ऐसे में खुदाई के बाद उन्हें सिर्फ अमरावती के अवशेष ही प्राप्त हुए। बाद में कॉलिन मेकेंजी ने भी इस स्तूप का भ्रमण किया लेकिन उनकी रिपोर्ट कुछ खास नहीं थी इसलिए छपी नहीं।
- 1854 ई. में गुंटूर (आंध्र प्रदेश) के कमिश्नर अमरावती यात्रा के समय कई उत्कीर्ण पत्थर और मूर्तियाँ अपने साथ मद्रास ले गए। इन्होंने अंत में अमरावती के स्तूप को बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप माना बताया।
- स्तूपों के उत्कीर्ण पत्थरों को 1850 के दशक में कई जगहों पर ले जाया गया। इस तरह मूर्तियों तथा उत्कीर्ण पत्थरों की लूट से अमरावती स्तूप नष्ट हो गया और साँची का स्तूप बचा रहा। इसका मुख्य कारण यह था कि साँची को संरक्षित किया गया था।
भारतीय मूर्तिकला
- बहुत से विद्वानों ने भारतीय-यूनानी शैली में बनी मूर्तियों के तुलनात्मक महत्ता को प्रविष्ट करने की कोशिश की।
- यूनानी-शैली में बनी बुद्ध तथा बोधित्व की मूर्तियों से यूरोपीय अधिक प्रभावित थे।
- तक्षशिला तथा पेशावर जैसे शहरों से बौद्ध धर्म से संबंधित कई मूर्तियाँ मिलीं। इनके अत्यधिक सुंदर और मूल्यवान होने के कारण ही ऐसी बहुत सी मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया।
मंदिर
- पहली शताब्दी में ही अलग-अलग धर्मों के देवताओं की मूर्तियाँ बनने लगीं और इन मूर्तियों को एक जगह स्थापित करने के लिए मंदिर बनाए जाने लगे। प्रारंभिक समय में ये मंदिर कुछ पहाड़ियों को काटकर उन्हें खोखला करके बनाए जाते थे। यह शैली मंदिर बनाने की सबसे प्राचीन शैली थी।
- ‘आजीवक’ संप्रदाय के संतों के लिए सम्राट अशोक द्वारा सबसे प्राचीन गुफा निर्मित की गई।
- मंदिर बनाने की सबसे प्राचीन शैली का सबसे अच्छा उदाहरण आठवीं सदी का ‘कैलाशनाथ मंदिर’ है। ताम्रपत्र अभिलेख में एलोरा के प्रभुख तक्षक द्वारा इसके निर्माण का जिक्र मिलता है।
- शुरुआत में मंदिर चौकोर आकार के बनाए गए, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इसमें भक्तों के लिए एक प्रवेश द्वार बना होता था जहाँ से वो मंदिर के अंदर जाते थे। बाद में गर्भगृह के ऊपर एक ढाँचा तैयार किया जाने लगा जिसे शिखर कहा गया।
समयावधि अनुसार घटनाक्रम
महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव
| क्रम संख्या | काल | घटना |
| 1. | लगभग 1500-1000 ई. पू. | प्रारंभिक वैदिक परंपराएँ |
| 2. | लगभग 1000-500 ई. पू. | उत्तर वैदिक परंपराएँ |
| 3. | लगभग छठी सदी ई. पू. | प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म |
| 4. | लगभग तीसरी सदी ई. पू. | आरंभिक स्तूप |
| 5. | लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से आगे | महायान बौद्ध मत का विकास, वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन परंपराएँ |
| 6. | लगभग तीसरी सदी ईसवी | सबसे पुराने मंदिर |
| 7. | उन्नीसवीं सदी 1814 | इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता की स्थापना। |
| 8. | 1834 | रामराजा लिखित एसेज ऑन द ऑर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन, कनिंघम द्वारा सारनाथ के स्तूप की छानबीन। |
| 9. | 1835-1842 | जेम्स फर्ग्युसन द्वारा महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण |
| 10. | 1851 | गवर्नमेंट म्यूजियम, मद्रास की स्थापना। |
| 11. | 1854 | अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा ‘मिलसा टोप्स’ का लिखा जाना, जो साँची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। |
| 12. | 1878 | राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक ‘बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि’ का प्रकाशन। |
| 13. | 1880 | एच एच कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया जाना। |
| 14. | 1888 | ट्रेजर-ट्रोव एक्ट का बनाया जाना। इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्त्व की किसी भी चीज को हस्तगत कर सकती थी। |
| 15. | बीसवीं सदी 1914 | जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे की ‘द मॉन्युमेंट्स ऑफ साँची’ पुस्तक का प्रकाशन। |
| 16. | 1923 | जॉन मार्शल की पुस्तक ‘कंजर्वेशन मैनुअल’ का प्रकाशन |
| 17. | 1955 | प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली की नींव का रखा जाना। |
| 18. | 1989 | साँची को एक विश्व कलादाय स्थान घोषित किया जाना। |
| कक्षा 12 इतिहास के अन्य अध्याय के नोट्स | यहाँ से प्राप्त करें |