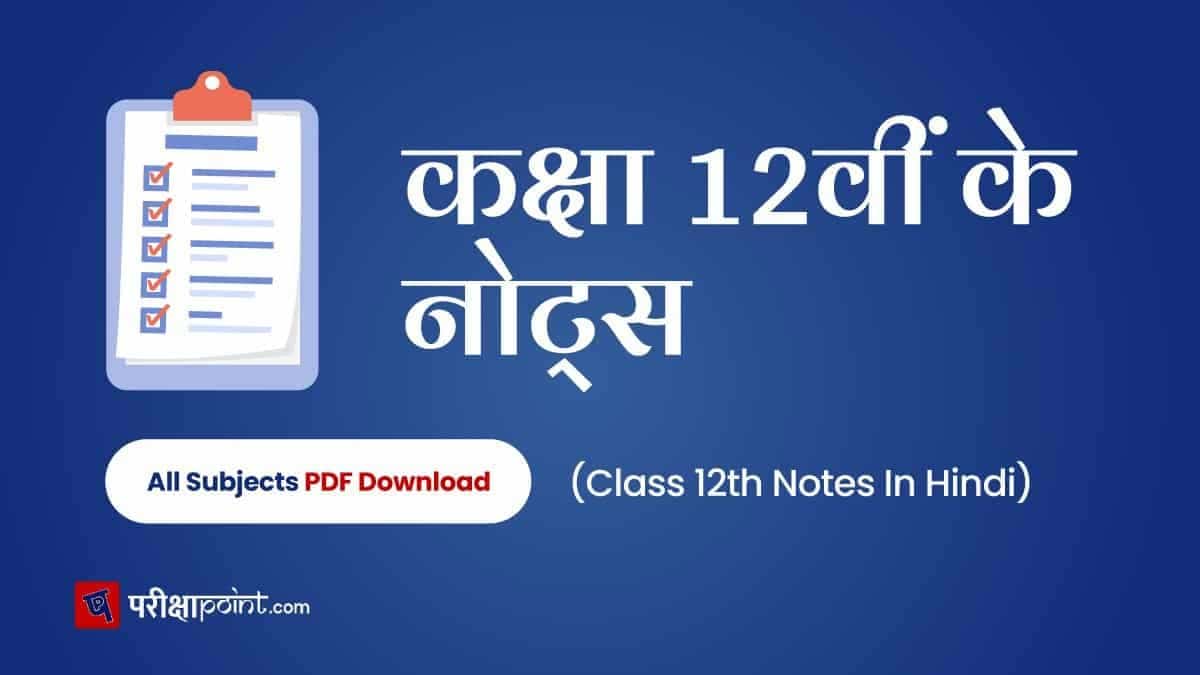इस लेख में छात्रों को एनसीईआरटी 12वीं कक्षा की भूगोल की पुस्तक-2 यानी भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अध्याय- 7 “परिवहन तथा संचार” के नोट्स दिए गए हैं। विद्यार्थी इन नोट्स के आधार पर अपनी परीक्षा की तैयारी को सुदृढ़ रूप प्रदान कर सकेंगे। छात्रों के लिए नोट्स बनाना सरल काम नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों का काम थोड़ा सरल करने के लिए हमने इस अध्याय के क्रमानुसार नोट्स तैयार कर दिए हैं। छात्र अध्याय- 7 भूगोल के नोट्स यहां से प्राप्त कर सकते हैं।
Class 12 Geography Book-2 Chapter-7 Notes In Hindi
आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दो ही तरह से ये नोट्स फ्री में पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने के लिए इस पेज पर बने रहें और ऑफलाइन पढ़ने के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें। एक लिंक पर क्लिक कर आसानी से नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए ये नोट्स बेहद लाभकारी हैं। छात्र अब कम समय में अधिक तैयारी कर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे, यह अध्याय पीडीएफ के तौर पर भी डाउनलोड हो जाएगा।
अध्याय- 7 “परिवहन तथा संचार“
| बोर्ड | सीबीएसई (CBSE) |
| पुस्तक स्रोत | एनसीईआरटी (NCERT) |
| कक्षा | बारहवीं (12वीं) |
| विषय | भूगोल |
| पाठ्यपुस्तक | भारत लोग और अर्थव्यवस्था |
| अध्याय नंबर | सात (7) |
| अध्याय का नाम | “परिवहन तथा संचार” |
| केटेगरी | नोट्स |
| भाषा | हिंदी |
| माध्यम व प्रारूप | ऑनलाइन (लेख) ऑफलाइन (पीडीएफ) |
कक्षा- 12वीं
विषय- भूगोल
पुस्तक- भारत लोग और अर्थव्यवस्था
अध्याय- 7 “परिवहन तथा संचार”
परिवहन के विभिन्न साधन
मनुष्य वस्तुओं, पदार्थों और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करता है, जिन्हें परिवहन का साधन कहते हैं। परिवहन के साधनों को निम्न तीन वर्गों में बाँटा गया है-
- स्थल परिवहन
- पुराने समय से ही कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता था।
- बाद में आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए सड़क और रेल परिवहन सुविधा पर ध्यान दिया जाने लगा।
- स्थल परिवहन के दो भाग निम्न प्रकार हैं-
- सड़क परिवहन
- भारतीय सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है।
- द्वितीय विश्व युद्ध से पहले आधुनिक प्रकार का सड़क परिवहन दुर्लभ था।
- आधुनिक सड़क निर्माण का पहला प्रयास वर्ष 1943 में ‘नागपुर योजना’ को आधार बनाकर किया गया।
- वर्ष 1961 में सड़कों की दशा सुधारने के लिए ‘बीस वर्षीय सड़क योजना’ शुरू की गई।
- वर्तमान समय में शाही राजमार्ग अमृतसर से कोलकाता के बीच विस्तृत है, जिसे दो भागों में बाँटा गया है-
- अमृतसर से दिल्ली (NH-1)
- दिल्ली से कोलकाता (NH-2)
- सड़कों को निर्माण तथा रखरखाव के उद्देश्य से निम्न भागों में बाँटा गया है-
- राष्ट्रीय महामार्ग
- राज्य महामार्ग
- जिला सड़के
- ग्रामीण सड़के
- अन्य सड़के
- रेल परिवहन
- रेल परिवहन की सुविधा ब्रिटिश काल में उपलब्ध हो गई थी।
- महात्मा गाँधी ने रेल के महत्व को उजागर करते हुए कहा था कि “भारतीय रेलवे ने विविद संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है।”
- वर्ष 1853 में भारतीय रेलवे की स्थापना मुंबई से थाणे के बीच हुई।
- भारतीय रेलवे को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है।
- रेल पटरियों की चौड़ाई के आधार पर इनके तीन वर्गों के नाम निम्नलिखित हैं-
- बड़ी लाइन
- मीटर लाइन
- छोटी लाइन
- सड़क परिवहन
- जल परिवहन
- यह यात्री और माल के वहन के लिए सबसे सस्ता साधन है।
- भारी सामानों के लिए उपयुक्त होने के साथ-साथ ईंधन-दक्ष तथा परिस्थितिकी अनुकूल परिवहन साधन है।
- जलिय परिवहन के दो प्रकार निम्न हैं-
- अंतःस्थलीय जलमार्ग
- रेल मार्गों के आने से पहले अंतःस्थलीय जलमार्ग परिवहन का मुख्य साधन था।
- इसके अंतर्गत मुख्य रूप से नदियों और नहरों को शामिल किया जाता है।
- वर्ष 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई।
- प्राधिकरण द्वारा तीन अंतःस्थलीय जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया और 10 अन्य जलमार्ग को केवल राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में पहचाना गया।
- भारत के मुख्य राष्ट्रीय जलमार्ग निम्न हैं-
- राष्ट्रीय जलमार्ग-1
- राष्ट्रीय जलमार्ग-2
- राष्ट्रीय जलमार्ग-3
- राष्ट्रीय जलमार्ग-4
- राष्ट्रीय जलमार्ग-5
- महासागरीय जलमार्ग
- भारत में द्वीपों के साथ-साथ लगभग 7517 कि.मी. लंबाई वाला विशाल समुद्र तट है।
- 12 प्रमुख एवं 185 गौण पत्तन महासागरीय मार्गों को संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवहन क्षेत्र में महासागरीय मार्गों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
- भार की दृष्टि से भारत में लगभग 95% और मूल्य की दृष्टि से 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ-साथ इन मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए भी किया जाता है।
- अंतःस्थलीय जलमार्ग
- वायु परिवहन
- एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए यह परिवहन का सबसे तीव्र साधन है।
- भारत में वायु परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में हुई थी।
- भारत ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस कंपनियों के माध्यम से वायु परिवहन को आसान बनाया है।
- पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन की सेवा उपलब्ध कराती है।
- वहीं पवन हंस लिमिटेड पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
- वर्तमान में कुछ निजी कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेवाएँ शुरू कर दी गई हैं।
तेल और गैस पाइप लाइन
- पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से गैस तथा तरल पदार्थों के परिवहन को आसान बनाया जाता है।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय के अधीन स्थापित ‘ऑयल इंडिया लिमिटेड’ द्वारा कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन से जुड़ा कार्य किया जाता है।
- ऑयल इंडिया लिमिटेड को वर्ष 1959 में कंपनी के रूप में स्वीकार किया गया था।
- एशिया की पहली 1157 कि.मी. लंबी देशपारीय पाइपलाइन का निर्माण आई.ओ.एल. द्वारा किया गया जिसे और आगे वर्ष 1966 में कानपुर तक विस्तारित किया गया।
- वर्तमान में 1265 कि.मी. लंबी एक पाइप लाइन सलाया से मथुरा तक बनाई गई है।
- अब ओ. आई. एल. द्वारा नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक 660 कि.मी. लंबी पाइप लाइन बनाने की प्रक्रिया चल रही है।
विस्तृत संचार जाल और संचार के साधन
- आरंभिक काल में मनुष्य सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए ढोल या पेड़ के खोखले तने को बजाते थे।
- प्राचीन कल में आग, धुआँ और तेज धवकों का प्रयोग भी संचार साधन के लिए किया जाता था।
- उस दौरान घोड़े, ऊँट, कुत्ते, कबूतर जैसे पशु-पक्षियों का प्रयोग संदेश पहुँचाने के लिए किया जाता था।
- प्राचीन काल में संचार के साधन ही परिवहन के साधन होते थे।
- आधुनिक काल में डाकघर, तार, प्रिंटिंग प्रेस, दूरभाष और उपग्रहों की खोज ने संचार को तेज गति प्रदान की साथ ही उसे आसान बना दिया।
- व्यक्ति संदेश पहुँचाने के लिए संचार की विभिन्न विधियों का उपयोग करता है। मानदंड एवं गुणवत्ता के आधार पर संचार साधनों को निम्न दो श्रेणियों में बाँटा गया है-
- व्यक्तिक संचार तंत्र
- व्यक्तिगत संचार तंत्रों में आधुनिक और सबसे उपयुक्त साधन इंटरनेट है।
- इंटरनेट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है।
- इस संचार तंत्र के अंतर्गत पत्रादि, टेलीफोन, तार, टेलीग्राम, फैक्स, ई-मेल, इंटरनेट इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है।
- उपयोगकर्ता ई-मेल के द्वारा ज्ञान तथा सूचना की दुनिया में सीधे संपर्क करते हैं।
- इंटरनेट का मौद्रिक लेन-देन के साथ-साथ ई-कॉमर्स का अधिकारिक रूप से प्रमुख माध्यम बन गया है।
- जनसंचार/सार्वजनिक संचार तंत्र- सार्वजनिक संचार तंत्र के साधन निम्नलिखित हैं-
- रेडियो
- भारत में रेडियों का प्रथम प्रसारण वर्ष 1923 में ‘रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे’ द्वारा किया गया था।
- रेडियों ने बहुत कम समय में लोगों के घरों में अपनी जगह बना ली थी।
- वर्ष 1930 में सरकार ने ‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम’ के अंतर्गत इस लोकप्रिय संचार माध्यम को अपने नियंत्रण में ले लिया।
- वर्ष 1936 को इसे ‘ऑल इंडिया रेडियो’ और वर्ष 1957 में ‘आकाशवाणी’ के रूप में बदल दिया गया।
- ऑल इंडिया रेडियो द्वारा सूचना, शिक्षा संसद व राज्य विधानसभाओं के विभिन्न सत्रों और मनोरंजन से जुड़े कई प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है।
- टेलीविजन/टी.वी
- शुरुआत में टेलीविजन सेवाएँ सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक सीमित थीं, जोकि वर्ष 1959 में दिल्ली में आरंभ की गई थीं।
- वर्ष 1976 में टी.वी. को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया और इसे दूरदर्शन के रूप में एक अलग पहचान दी गई।
- राष्ट्रीय टेलीविजन डी डी-1 के चालू होने के बाद राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिसका विस्तार देश भर के पिछड़े और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक किया गया।
- उपग्रह
- उपग्रह संचार की एक महत्वपूर्ण विधा है, जोकि संचार के अन्य साधनों का भी नियमन करता है।
- इसके माध्यम से प्राप्त चित्रों का मौसम के पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सीमा क्षेत्रों की निगरानी इत्यादि में उपयोग किया जाता है।
- भारत की उपग्रह प्रणाली को समाकृति एवं उद्देश्यों के आधार पर दो भागों ‘इंडियन नेशनल सेटेलाइट सिस्टम’ (इनसैट) और ‘इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम’ (आई आर एस) में बाँटा गया है।
- इनसैट एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है, जिसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी।
- भारत द्वारा आई आर एस उपग्रह प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1988 में रूस के वैकानूर से आई आर एस-1ए प्रक्षेपण के साथ शुरू हुई थी।
- कुछ समय बीतने के बाद भारत ने स्वयं का प्रक्षेपण वाहन ‘पोलर सैटेलाइट लाँच वेहकिल’ (पी एस एल वी) विकसित किया।
- रेडियो
- व्यक्तिक संचार तंत्र
| PDF Download Link |
| कक्षा 12 भूगोल के अन्य अध्याय के नोट्स | यहाँ से प्राप्त करें |